 फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books




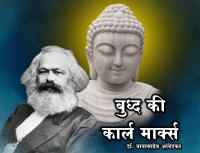


Top News








Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,ब्राह्मणवाद की विजय : राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म (भाग 10) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर
बहिष्कृतों के बारे में मनु के नियम निस्संदेह अन्यायपूर्ण और अमानवीय हैं। कोई यह कह सकता है कि यह कोई बहुत विलक्षण बात नहीं। इसका कारण यह है कि ये नियम धर्मविमुखता और धर्मद्रोह संबंधी नियमों की तरह हैं, जो सभी धर्म-संहिताओं में मिलते हैं। दुर्भाग्य से यह सच है । बौद्ध धर्म को छोड़कर प्रत्येक धर्म ने अपनी-अपनी संहिता में अटूट निष्ठा रखने और तद्नुसार आचरण करने पर बल देने के लिए उत्तराधिकार केनियमों का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग किया है। सम्राट कांस्टैंटीन्स और जुलियन ने ईसाई व्यक्ति को यहूदी धर्म अपनाने या विधर्मी बन जाने या कोई और धर्म अपनाने पर दंडित किया। सम्राट थियोडोसियस और वैलेंटीनियोस ने धर्म प्रचारकों के लिए, यदि वे उसी प्रकार अन्याय से दूसरों को पथभ्रष्ट करने का साहस करते हैं, तो मृत्युदंड तक देने की व्यवस्था की थी। यूरोप के अन्य देशों¹ में दंड विधान की यही पद्धति अपने यहां ईसाई धर्म लागू करने के लिए अपनाई गई।

बहिष्कृत व्यक्ति संबंधी कानून के बारे में ऐसा दृष्टिकोण अपनाना ओछी बात है। सबसे पहली बात तो यह कि किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने की प्रथा को ब्राह्मणवाद ने जन्म दिया। यह पद्धति जाति प्रथा के कारण उत्पन्न हुई। ब्राह्मणवाद ने जातिप्रथा को जन्म देने का जब एक बार निश्चय कर लिया, तब बहिष्कृत व्यक्तियों के बारे में ऐसा नियम बनाना आवश्यक ही था। बहिष्कृत व्यक्ति को दंडित कर ही जातिप्रथा लागू की जा सकती थी । दूसरे, ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म के धर्मविमुखता संबंधी नियमों और ब्राह्मणवाद के जाति संबंधी नियमों में अंतर है। ईसाई या मुसलमान धर्म में विधर्मी होने का अर्थ, धर्म में आस्था न रखने या धर्म का गलत निर्वचन करने तक सीमित था। ब्राह्मणवाद में विधर्मी होने का संबंध धार्मिक आस्था नहीं होने या उसका अभाव हो जाने से बिल्कुल भी नहीं था। इसका संबंध एक सामाजिक संस्था, अर्थात् जातिप्रथा को मानने या न मानने से था । इस जाति से बाहर चले जाने को दंडनीय समझा गया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है।
ब्राह्मणवाद धर्म के बहिष्कृत व्यक्ति संबंधी नियमों की तुलना अगर अन्य धर्मों के विधर्मिता संबंधी नियमों से की जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म में ईश्वर में आस्था रखना आवश्यक नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखना ब्राह्मणवाद में आवश्यक नहीं है, सदाचार के द्वारा मुक्ति या ईश्वर के दूत में विश्वास रखना ब्राह्मण धर्म में आवश्यक नहीं है, लेकिन वेदों की पवित्रता में विश्वास रखना ब्राह्मणवाद में आवश्यक है। केवल यही एक चीज है जो ब्राह्मणवाद में आवश्यक है। केवल जाति का उल्लंघन ही दंडनीय है। बाकी अन्य का उल्लंघन किया जा सकता है।
जो लोग एकीकरण की इन शक्तियों को देखते-समझते हैं, वे यह स्वीकार करेंगे कि अंतर्जातीय विवाह या सहभोज का निषेध करना समाज को तोड़ देने के बराबर है। यह एकता के लिए मौत का पैगाम है, एकजुट होकर काम करने के रास्ते में एक जबरदस्त बाधा है। हम आगे चलकर देखेंगे कि ब्राह्मणवाद गैर-ब्राह्मणों द्वारा इसे उखाड़ फेंकने के लिए हर संयुक्त कार्रवाई को विफल करने के बारे में सचेत था । और इसीलिए उसने भारतीय समाज को इस प्रकार वर्गों में विभाजित किया। लेकिन किसी भी विष का प्रभाव
1. देखिए, लॉज ऑफ इंग्लैंड पर स्टीफन की टीका (15वां संस्करण), खंड 4, पृ. 179
उसका प्रयोग करने वाले के मूल उद्देश्य तक सीमित नहीं रह सकता। यही जाति के मामले में भी हुआ। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के विरुद्ध गैर-ब्राह्मणों को पंगु बना देना चाहता था, उसकी योजना उन्हें राष्ट्र के रूप में विदेशी शक्ति के विरुद्ध पंगु बना देने की नहीं थी। लेकिन जाति रूपी विष का परिणाम यह है कि उनमें ब्राह्मणवाद के ही नहीं, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध भी सिर उठाने की शक्ति नहीं रह गई। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणवाद ने जातिप्रथा को जन्म देकर राष्ट्रीयता के विकास को भी महान क्षति पहुंचाई।
चाहे लोग कुछ भी कहें, हिंदू जातिप्रथा में किसी भी दोष को स्वीकार नहीं करेगा और एक दृष्टि से यह सही भी है। प्रत्येक परिवार में उसके सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, एकता और सहायता करने की भावना होती है। चोरों में भी एक-दूसरे के सामान्य हितों के प्रति सद्भाव होता है। डाकुओं के गिरोह में सब का एक ही स्वार्थ होता है और सब एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं। इनके गिरोह चाहे एक-दूसरे के विरोधी क्यों न हों, तब भी इनमें परस्पर भाईचारे और अपने-अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होती है। और इसी से ये पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जाति में वे सभी गुण होते हैं जो किसी समाज में होने चाहिए।
इसमें परस्पर प्रेम, एकता और एक-दूसरे की सहायता करने की प्रबल भावना होती है जो किसी परिवार के गुण कहे जाते हैं। चोरों जैसी बंधुत्व की भावना का इसे श्रेय प्राप्त है। इसमें निष्ठा और भाईचारे की यह भावना भी होती है, जो हमें भिन्न-भिन्न गिरोहों में मिलती है और इसमें समान हित या स्वार्थ की वह भावना भी होती है, जो डाकुओं में मिलती है।
जाति में इन प्रशंसनीय गुणों के होने के कारण हिंदू गौरव का अनुभव कर सकता है और यह कह सकता है कि 'जाति' में कोई दोष नहीं होता। लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसकी जाति के बारे में यह धारणा, कि यह सामाजिक संगठन का एक आदर्श रूप है, जो इस अनुमान या कल्पना पर आश्रित है कि प्रत्येक जाति अपने आपको एक स्वतंत्र समाज कह सकती है, यही उसका लक्ष्य है, जैसा कि किसी राष्ट्र के संबंध में होता है। लेकिन जब हम हिंदू समाज और उसी के अनुरूप जातिप्रथा पर विचार करते हैं, तब यह सिद्धांत अर्थहीन हो जाता है।
यहां तक कि इस विषय पर विचार करते समय हिंदू यह कभी नहीं स्वीकार करेगा कि जातिप्रथा एक बुरी प्रथा है। आप हिंदुत्व को जातिप्रथा के दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराएं, तब हिंदू तुरंत कह उठेगा कि 'यूरोप में भी वर्ग प्रणाली ( क्लास सिस्टम) है।' इस प्रतिक्रिया का आशय अगर यह है कि दार्शनिकों का ऐसा समाज तो कहीं नहीं है, जहां मूलभूत एकता हो, सबका एक जैसा उद्देश्य हो, परस्पर सहानुभूति हो, सार्वजनिक हित के प्रति निष्ठा हो और सबके कल्याण की चिंता हो। अगर हिंदू यह कहे कि प्रत्येक समाज में ऐसे परिवार और वर्ग होते हैं, जहां अलगाव, संदेह और ईर्ष्या उन्हीं परिवारों और वर्गों की भाँति पाई जाती है, जहां डाकुओं के गिरोह, गुटबाजी, संकीर्ण दलबंदी, ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, कार्तेल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राजनैतिक पार्टियां होती हैं, तो किसी को क्या शिकायत हो सकती है। इनमें से कुछ स्वार्थ और लूटने के कारण आपस में संगठित होती हैं और बाकी ऐसी जो जनता की सेवा करने का उद्देश्य लेकर उठ खड़ी होती हैं, लेकिन वह उसको अपना शिकार बनाने में कोई संकोच नहीं करतीं।
यह स्वीकार किया जा सकता है कि हर जगह वास्तविक समाज पूर्ण रूप से एक नहीं होता, बल्कि उसमें छोटे-छोटे वर्ग होते हैं, जिनकी अपनी-अपनी समस्याएं होती हैं। और ये समस्याएं उन तात्कालिक और विशिष्ट प्रयोजनों से प्रेरित होती हैं। लेकिन हिंदू अपनी जाति व्यवस्था और गैर-हिंदू वर्ग प्रणाली के बीच इस समानता को अपनी ढाल नहीं बना सकता और उसके पीछे दुबक कर बैठा नहीं रह सकता जैसे इस विषय पर और कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। सच तो यह है कि इससे भी बड़ा प्रश्न है, जिसका उसे उत्तर देना है। उसे इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि हालांकि हर समाज में वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे समाज हैं जिनमें वर्ग असामाजिक होते हैं और कुछ ऐसे भी समाज हैं जिनमें वर्ग समाज -विरोधी होते हैं। वर्ग-प्रणाली वाले समाज और जाति-प्रणाली वाले समाज में अंतर सिर्फ इस बात में है कि वर्ग-प्रणाली सिर्फ गैर-सामाजिक होती है, लेकिन जाति-प्रणाली तो निश्चित रूप से समाज - विरोधी है।
यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी समाज में वर्ग-प्रणाली गैर - सामाजिक भावना को क्यों पैदा करती है और दूसरे समाज में समाज - विरोधी भावना क्यों पैदा करती है। इसका जो स्पष्टीकरण प्रोफेसर जॉन डेवी ने दिया है, उससे अधिक अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। उनके मतानुसार हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि ये वर्ग अलग-अलग हैं या एक-दूसरे से संबद्ध हैं। क्या ये एक-दूसरे के हितों के बारे में ख्याल रखते हैं, या उनमें इस भावना का अभाव है। अगर ये वर्ग एक-दूसरे से संबद्ध है, अगर इनमें एक-दूसरे के हितों के बारे में ख्याल नहीं है तब उनमें एक-दूसरे के प्रति सिर्फ गैर-सामाजिक भावना होगी। अगर इन वर्गों एक-दूसरे के हित के बारे में ख्याल नहीं है तब इनमें समाज -विरोधी भावना होगी। प्रोफेसर डेवी¹ के शब्दों में:
1. डेमोक्रेसी एंड एजूकेशन, पृ. 99
“दल या गुट की अपनी पृथकता और एकांतता के कारण समाज-विरोधी भावना व्याप्त हो जाती है। और जहां भी किसी का स्वार्थ अपने तक सीमित होता है, वहां ऐसी ही भावना पाई जाती है। इससे उसका पूर्ण संपर्क दूसरे वर्गों के साथ नहीं रहता और उसका मुख्य उद्देश्य पुनर्गठित और संपर्क द्वारा प्रगति करने के बजाए उसी की रक्षा करना रह जाता है, जो उसके पास पहले से ही है। यह भावना राष्ट्रों को एक-दूसरे से अलग कर देती है। इसी प्रकार जो परिवार अपने घरेलू मामलों में उलझे रहते हैं, जैसे उनका व्यापक जीवन में कोई संबंध न हो, स्कूल भी तब अलग जा पड़ते हैं, जब उनका घर और समुदाय से कोई संबंध न हो, स्कूल भी तब अलग जा पड़ते हैं, जब उनका घर और समुदाय से कोई संबंध नहीं रहता, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित में भेद बढ़ जाता है। मुख्य बात यह है कि पृथकता से जीवन संकीर्ण और औपचारिक मात्र रह जाता है, वर्ग में उसके आदर्श जड़ और स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं। "
प्रश्न यह है कि क्या समाज में वर्ग हैं या समाज एक संपूर्ण इकाई होता है। प्रश्न यह है कि विभिन्न वर्गों में परस्पर साहचर्य, सहयोगात्मक संपर्क और संबंध किस मात्रा से हद तक रहता है। उनके ऐसे कौन से उद्देश्य हैं, जिनमें वे प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे सहभागी रहते हैं। अन्य संस्थाओं के साथ संबंध रखने में वे कितने मुक्त हैं? कोई समाज इसलिए अवांछनीय नहीं है कि उसमें कई वर्ग हैं। यह तब अवांछनीय हो जाता है जब उनके वर्ग अलग-अलग हो जाते हैं। हर वर्ग की अपनी कार्यशैली होती है। इसी से अलग-अलग रहने की प्रवृत्ति समाज - विरोधी भावना का पैदा होना संभव हो जाता है।
वर्गों में एक-दूसरे से अलग - अलग रहना ब्राह्मणवाद के कारण हुआ। इसके लिए ब्राह्मणवाद ने प्रमुखतः जो कार्य किया, अंतर्जातीय विवाह और सहभाज की प्रणाली को समाप्त करना था, जो प्राचीन काल में चारों वर्णों में प्रचलित थी। इस बारे में हम इस अध्याय के पहले खंड में चर्चा कर चुके हैं। इस वृत्त का एक भाग कहा जाना बाकी है। मैं कह चुका हूं कि वर्ण-व्यवस्था का विवाह से कोई संबंध नहीं था। और विभिन्न वर्गों पुरुष और स्त्रियां आपस में विवाह कर सकते थे और उन्होंने किया भी। कानून अंतर्वर्ण विवाह के रास्ते आड़े नहीं आता था। इन विवाहों का विरोध समाज में नैतिकता की दृष्टि से भी नहीं होता था। सवर्ण विवाह करना न तो कानूनन जरूरी समझा जाता था और न समाज ही इस पर बल देता था। इस बात के बावजूद कि वर की अपेक्षा वधू उच्च वर्ण की है या वर उच्च वर्ण का है और वधू निम्न वर्ण की है, विभिन्न वर्गों के सभी विवाह वैध होते थे। वास्तव में जैसा कि प्रो. काणे कहते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के अंतर को कोई नहीं जानता था और स्थिति यह थी कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों, अर्थात् उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष के बीच विवाह पर रोक लगा दी। यह वर्णों के बीच आपसी संबंध को समाप्त करने और इनमें एक-दूसरे के प्रति गैर - भावना पैदा करने की दिशा में एक कदम था। लेकिन जहां प्रतिलोम विवाह के द्वारा अंतः संबंधों का द्वार खुला रखा गया, उसे बंद किया गया। जैसा कि क्रमिक असमानता विषयक खंड में कहा गया है, ब्राह्मणवाद ने अनुलोम विवाह, अर्थात् उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री के बीच विवाह जारी रखा। अनुलोम विवाह बहुत अच्छा नहीं कहा गया और यह सिर्फ एक ओर जाने का द्वार था, तो भी यह एक-दूसरे को मिलाने वाला द्वार था जिसके माध्यम से वर्णों का एक-दूसरे से बिल्कुल अकेले होने से रोकना संभव था। लेकिन यहां पर भी ब्राह्मणवाद ने चाल चली, जिसे ओछापन ही कहा जाएगा। यह कार्य कितना ओछा था, उन नियमों का यहां बताना आवश्यक है जो शिशु की स्थिति निर्धारित करने के लिए बनाए गए। प्राचीन काल से चले आ रहे नियमों के अधीन शिशु की स्थिति उसके पिता के आधार पर निर्धारित की जाती थी। मां के वर्ण का कोई महत्व नहीं था ।
निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी :
|
पिता का |
पिता का |
मां का नाम |
मां का वर्ण |
शिशु का नाम |
शिशु का वर्ण |
||
| 1. | शांतनु | क्षत्रिय | गंगा | शूद्र | भीष्म | क्षत्रिय | |
| 2. | शांतनु | क्षत्रिय | मत्स्यगंधा (धीवर) |
अनामिका | विचित्र वीर्य | क्षत्रिय | |
| 3. | पाराशर | ब्राह्मण | मत्स्यगंधा (धीवर) |
शूद्र | कृष्ण - द्वैपायन | ब्राह्मण | |
| 4. | विश्वामित्र | क्षत्रिय | मेनका | अप्सरा | शकुंतला | क्षत्रिय | |
| 5. | ययाति | क्षत्रिय | देवयानी | ब्राह्मण | यदु | क्षत्रिय | |
| 6. | ययाति | क्षत्रिय | शर्मिष्ठा (अनार्य) |
आसुरी | द्रुह्य | क्षत्रिय | |
| 7. | जरत्कारू | ब्राह्मण | जरत्कारि (अनार्य) |
नाग | असित | ब्राह्मण |
यह नियम पितृ-सवर्ण्य का नियम कहलाता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह-पद्धतियों पर इस पितृ-सवर्ण्य नियम के प्रभाव का विवेचन एक रोचक विषय है।
प्रतिलोम विवाह का प्रभाव यह होगा कि उच्च वर्ग की माताओं के बच्चे नीचे के वर्ण के कहलाएंगे, जो उनके पिता का है। अनुलोम विवाह पर इसका प्रभाव उलटा होगा । नीचे के वर्ण की माताओं के बच्चे ऊंचे वर्ण के कहलाएंगे, जो उनके पिता का वर्ण है।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -



