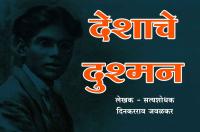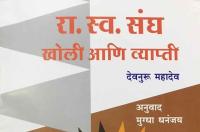फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
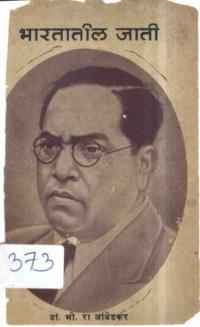
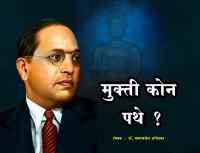
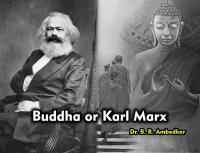
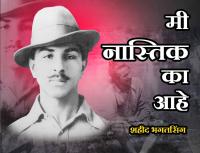
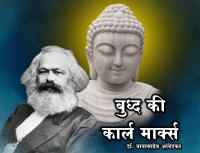
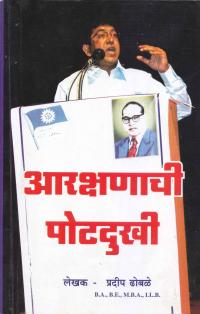

Top News


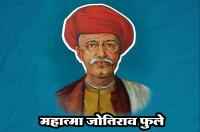


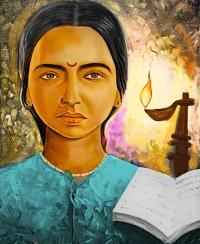
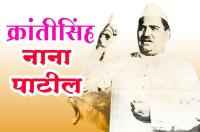
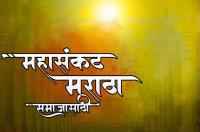
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,भारत में जातिप्रथा - उसकी संरचना, उत्पत्ति और विकास - लेखक - डॉ. भीमराव अम्बेडकर (भाग 3)
भारत में जातिप्रथा के प्रचलन और संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करते हुए अगला प्रश्न यह है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इसके मूल का प्रश्न एक कड़वा प्रश्न है और जातपांत के अध्ययन में इसकी दुखद अवहेलना की गई है; कुछ ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने इस प्रश्न पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया है। कुछ लोग समझ पाने में सफल रहे हैं कि यह जातपांत का मूल कहां हो सकता है। वे कहते हैं - "यदि हम मूल के प्रति अपनी स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें उसके बहुवचन रूप, अर्थात 'जातपांत के मूल का प्रयोग करना चाहिए।" वैसे भारत में जातपांत के मूल के बारे में कोई उलझन पेश नहीं हुई है, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि सजातीय विवाह ही जातपांत का एकमात्र कारण है और जब मैं जाति के मूल की बात कहता हूं तो इसका अर्थ सजातीय विवाह प्रथा की क्रियाविधि के मूल से है ।
किसी समाज में व्यक्तियों की अतिसूक्ष्म अवधारणा को इतने शक्तिशाली ढंग से प्रचारित करना मैं गंदगी उछालना कहने जा रहा था यह राजनीतिक भाषा में कोरी बकवास है। यह बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। समाज सर्वथा वर्गों से मिलकर बनता है; इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर बल देना अतिश्योक्ति हो सकती है, परंतु यह सच है कि समाज में कुछ निश्चित वर्ग होते हैं और उनके आधार भिन्न हो सकते हैं। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं। लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग से संबद्ध होता है। यह एक शाश्वत सत्य है और आरंभिक हिन्दू समाज भी इसका अपवाद नहीं रहा होगा। जहां तक हम जानते हैं, वह अपवाद नहीं था । यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखें तो पाते है कि जातपांत की उत्पत्ति के अध्ययन में यह बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि वह कौन सा वर्ग था, जिसने सबसे पहले अपनी जाति की संरचना की। इसलिए वर्ग और जाति एक-दूसरे के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जाति अपने को सजातीय परिधि में रखने वाला वर्ग है।

जातिप्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि वह कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि का सूत्रपात किया, जो इसका चक्रव्यूह है? यह प्रश्न बहुत कौतुहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जातिप्रथा कैसे पनपी और दृढ़ होती गई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं हैं। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूं। मैंने अभी कहा है कि विचाराधीन रीति-रिवाज हिन्दू समाज में प्रवाहित हैं। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए, ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति, अर्थात् ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिन्दु समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है और गैर- ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया, जहां इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और न संपूर्णता । यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गैर-ब्राह्मण जातियां इस प्रथा का अनुसरण करती हैं, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, तो यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति-व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली, यह एक अलग प्रश्न है, जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इस रीति-नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था । उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींच डाली और इसे जिंदा रखा।
अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूं, जिसका संबंध पूरे भारत में जातपांत के उद्भव और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है, वह यह कि देश के अन्य गैर-ब्राह्मण समुदायों में यह प्रथा कैसे फैली ? इसके उत्तर में मेरा विचार है कि पूरे भारत में जातिप्रथा के प्रचलन से ज्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मैं समझता हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और सूत्रपात दो अलग-अलग बातें नहीं हैं। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जातिप्रथा या तो भोले-भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रही।
पहले मैं भारत के विधि-निर्माता के बारे में बताना चाहूंगा। हर देश में उसके विधि- निर्माता होते हैं, जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि-निर्माता कानून और नैतिकता की प्रतिस्थापना करते हैं। भारत के विधि-निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है, तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की तो मैं कहता हूं कि वह एक दुःसाहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्य किया, वह वर्तमान-काल की मानवता से भिन्न थी । यह अकल्पनीय है कि जाति-विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। यदि वह क्रूर न होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता, जो उसकी 'व्यवस्था' में साफ झलकता है। मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूं परंतु यह निश्चित है कि मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किन्तु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया ओर न वह ऐसा कर सकता था। जातिप्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी। वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिन्दू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता। प्रचलित जातिप्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया । जातिप्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता । तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति-संरचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहता, सिवाय यह कहने के कि वैचारिक दृष्टि से यह गलत और इरादतन दुर्भावनापूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, और मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि वे हैं भी, परंतु गैर-ब्राह्मण अन्य जन-समुदायों पर जातिप्रथा थोपना उनके बूते के बाहर की बात थी। अपने इस तरह के दर्शन द्वारा, हो सकता है, उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने में सहायता की हो, परंतु अपनी क्षमता से वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं करा सकते थे। चाहे कोई कितना भी गौरवशाली हो । चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों न हो। अपने ढंग से समाज को चलाने में वह प्रशंसित तो हो सकता है, किन्तु यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरी आलोचना की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह असत्य नहीं है। पुरातन पंथी हिन्दुओं के मन में यह दृढ़ धारणा है कि हिन्दू समाज किसी तरह जातिप्रथा की प्रणाली में ढल गया और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है, बल्कि उसे इस आधार पर न्यायसंगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति सुखद हो सकती है, क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर इस आधार पर ही ध्यान नहीं दिलाया है कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गई, न ही मैं उन सुधारकों का पक्षधर हूं, जो इसके विरूद्ध है। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी है और न ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की निस्सारता बताना चाहता हूं, जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है।
इस तरह व्यक्ति-पूजा का सिद्धांत भारत में जातिप्रथा के प्रचलन के निराकरण में बहुत लाभदायक साबित नहीं होता। पश्चिमी विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति - को विशेष महत्व नहीं दिया लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्याओं को आधार बना लिया। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जातिप्रथा को जन्म दिया, वे हैं (1) व्यवसाय, ( 2 ) विभिन्न कबायली संगठनों का प्रचालन, ( 3 ) नई धारणाओं का जन्म ( 4 ) संकर जातियां, और (5) आव्रजन ।
प्रश्न यह उठता है कि क्या वे मान्यताएं अन्य समाजों में मौजूद नहीं हैं और क्या भारत में ही उनका विशिष्ट रूप विद्यमान है। यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरे विश्व में एक समान हैं, तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ ली? क्या इसका कारण यह है कि वे देश वेदों की इस भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र हैं या विद्वान गलती पर हैं? मैं सोचता हूं कि बाद की बात सही है।
अनेक लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी-अपनी विचाराधारा के समर्थन में उच्च सैद्धांतिक मूल्यों के दावे किए हैं। कोई विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि गहराई से देखने पर प्रकट होता है कि ये सिद्धांत उदाहरणों के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि इसमें "महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं।" सर डेनजिल इब्बतसन, नेसफील्ड, सेनार और सर एच. रिजले के सिद्धांत यहीं हैं। मोटे तौर पर इनकी आलोचना में यह कहा जा सकता है कि यह एक लीक पीटने का प्रयत्न है। नेसफील्ड उदाहरण प्रस्तुत करते हैं- "सिर्फ कार्य, केवल कार्य ही वह आधार था, जिस पर भारत की जातियों की पूर्ण प्रथा का निर्माण हुआ।" लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह इस कथन से हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं करते, जिसका सार यही है कि भारत में जातियों का आधार व्यवसाय मात्र है और यह स्वयं में एक लचर दलील है। हमें नेसफील्ड महोदय से इस सवाल का जवाब चाहिए कि यह कैसे हुआ कि विभिन्न व्यवसायी वर्ग विभिन्न जातियां बन गए? मैं अन्य नृजाति-विज्ञानियों के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए सहर्ष प्रसन्न होता, यदि यह सही न होता कि नेसफील्ड का सिद्धांत एक अजीब सिद्धांत है।
मैं इन सिद्धांतों की आलोचना जारी रखते हुए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि जिन सिद्धांतों ने जातिप्रथा को विभाजनकारी नियमों के पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताया है, जैसाकि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकास के सिद्धांत में व्याख्या की है और इसे स्वाभाविक बताया है तथा इसे 'जैविक संरचना भेद' कहकर लचर पुरातन पंथी शब्द जाल की धारणाओं को पुष्ट किया है या सुजनन-विज्ञान के आदि प्रयत्नों का समर्थन किया है, जिससे उसकी सनक का आभास विदित होता है कि जातिप्रथा अवश्यंभावी है या विधि सम्मत है, यह जानकर निरीह वर्गों पर सजंग होकर इन निमयों को आरोपित किया गया है।
यह उचित ही रहेगा कि शुरू में मैं यह बात याद दिलाऊं कि अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी चार वर्णों में विभाजित था, ये हैं (1) ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, (2) क्षत्रीय या सैनिक वर्ग, (3) वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, और (4) शूद्र अथवा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था और इसीलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी। हिन्दू इतिहास में किसी समय पुरोहित वर्ग ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और इस तरह स्वयं सीमित प्रथा से जातियों का सूत्रपात हुआ। दूसरे वर्ण भी समाज विभाजन के सिद्धांतानुसार अलग-अलग खेमों में बंट गए। कुछ का संख्या बल अधिक था तथा कुछ का नगण्य । वैश्य और शूद्र वर्ण मौलिक रूप से वे तत्व हैं, जिनकी जातियों की अनगिनत शाखा, प्रशाखाएं कालांतर में उभरी हैं। क्योंकि सैनिक व्यवसाय के लोग असंख्य समुदायों में सरलता से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए यह वर्ण सैनिकों और शासकों के लिए सुरक्षित हो गया।
समाज का यह उप-वर्गीकरण स्वाभाविक है । किन्तु उपरोक्त विभाजन में अप्राकृतिक तत्व यह है कि इससे वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे संकुचित बनते चले गए, जिन्होंने जातियों का रूप ले लिया। प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें अपने दायरे में रहने के लिए विवश किया गया और उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया या उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। मेरा कहना है कि इसका द्विपक्षीय उत्तर है कुछ ने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरे के द्वार अपने लिए बंद पाए। पहला पक्ष मनोवैज्ञानिक है और दूसरा चालाकी भरा, परंतु ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं और जाति- संरचना की संपूर्ण रीति-नीति में दोनों की व्याख्या जरूरी है।
मैं पहले मनोवैज्ञानिक व्याख्या से शुरू करता हूं। इस संबंध में हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि औद्योगिक, धार्मिक या अन्य कारणों से वर्ग अथवा जातियों ने अपने आपको आत्म- केंद्रित या सजातीय विवाह की प्रथा में क्यों बांध लिया? मेरा कहना है कि ब्राह्मणों के करने के कारण ऐसा हुआ। सजातीय विवाह या आत्म-केंद्रित रहना ही हिन्दू समाज का चलन था और क्योंकि इसकी शुरूआत ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए गैर-ब्राह्मण वर्गों अथवा जातियों ने भी बढ़-चढ़कर इसकी नकल की और वे सजातीय विवाह प्रथा को अपनाने लगे। यहां यह खरबूजे को देखकर खरबूजे की रंग बदलने वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसने सभी उप-विभाजनों को प्रभावित किया। इस तरह जातिप्रथा का मार्ग प्रशस्त हुआ। मनुष्य में नकलबाजी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस कारण भारत में जातिप्रथा के जन्म की यह व्याख्या पर्याप्त है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि बाल्टर बागेहोट को कहना पड़ा "हमें यह नहीं सोचना चाहिए .... कि यह नकलबाजी स्वैच्छिक होती है या इसके पीछे कोई भावना काम कर रही होती है। इसके विपरीत, इसका जन्म मानव के अवचेतन मन में होता है और पूर्ण चेतना जागने पर उसके प्रभावों का आभास होता है। इस तरह इसके तत्काल उदय का प्रश्न नहीं है, बल्कि बाद में भी इसका अहसास नहीं होता है। दरअसल, हमारी नकल करने की प्रवृत्ति का स्रोत विश्वास होता है और ऐसे कारण हैं, जो पूर्वकालीन रूप से हमें यह विश्वास कराते हैं तथा हमें विश्वास करने से विरक्त करते हैं यह हमारी प्रकृति के अस्पष्ट भाग हैं। सरल मन से नकल करने की प्रवृत्ति पर कोई संदेह नहीं हैं।"3 नकल करने की इस प्रवृत्ति के विषय को गेबरिल टार्डे ने वैज्ञानिक अध्ययन का रूप दिया, जिन्होंने नकल करने की प्रवृत्ति को तीन नियमों में बांटा है। उसके तीन नियमों से एक है कि नीचे वाले ऊपर की नकल करते हैं। उन्हीं के शब्दों में " अवसर मिलने पर दरबारी सदा अपने नायकों, अपने राजा या अधिपति की नकल करते हैं और आम जनता भी उसी प्रकार अपने सामंतों की नकल करती है।" 4 नकल के बारे में टार्डे का दूसरा नियम है कि चाहे आदर्श पात्र और अनुसरणकर्ता के बीच कितनी ही दूरी क्यों न हो, उनके अनुसार नकल करने की इच्छा और तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं के शब्दों में, "जिस व्यक्ति की नकल की जाती है, वह होता है हमारे बीच सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति या समाज। दरअसल, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे हमारा अंतर कितना ही हो यदि हम उनसे सीधे संपर्क में आते हैं तो उनका संसर्ग अत्यंत प्रभावोत्पादक होता है। अंतर का अर्थ समाज - विज्ञान के आधार पर लिया गया है। यदि हमारा उनसे प्रतिदिन बार-बार संसर्ग होता है और उनके जैसे रंग-ढंग अपनाने का अवसर मिलता है, तो वह व्यक्ति चाहे हमसे कितने की ऊंचे स्तर का क्यों न हो, कितना ही अपरिचित हो, फिर भी हम स्वयं को उसके निकट मानते हैं। सबसे कम दूरी पर निकटतम व्यक्ति के अनुसरण का नियम प्रकट करता है कि ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति निरंतर सहज प्रभाव छोड़ते हैं।"5
3. फिजिक्स एंड पालिटिक्स (भौतिकी एवं राजनीति शास्त्र) 1915, पृष्ठ 60.
4. लॉज आफ इमीटेशन (नकल करने के सिद्धांत) अनुवाद ई.सी. पार्सन्स, पृष्ठ 217.
5. तथैव पृष्ठ 225.

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -