 फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
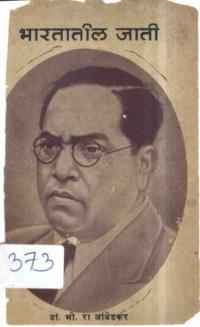
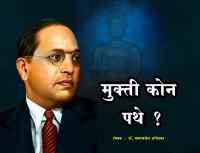
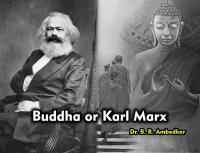
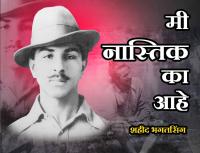
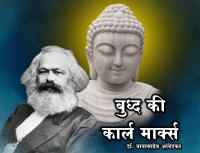
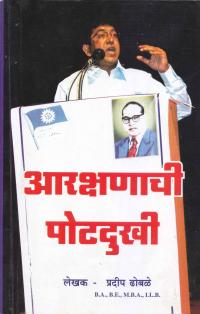

Top News

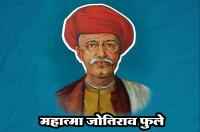


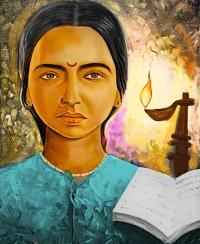

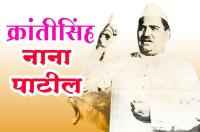
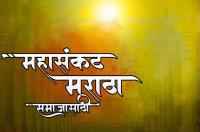
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,हिंदू धर्म की पहेलियां - ( भाग ४२ ) लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर
परिशिष्ट - 2
वेदांत की पहेली
प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने षट्दर्शन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसमें वास्तव में सबसे विख्यात है वेदांत दर्शन। केवल नाम के कारण ही नहीं, बल्कि हिंदुओं में इसकी जितनी मान्यता है, उतनी अन्य दर्शनों की नहीं। वेदों के प्रत्येक अनुयायी को वेदांत पर गर्व है। वह केवल इसको मानता ही नहीं बल्कि वह यह भी समझता है विश्व को दार्शनिक विचारों के योगदान में यह सर्वाधिक मूल्यवान है। वह समझता है कि वेदांत दर्शन वेदों की शिक्षा का लक्ष्य है। उसे कभी भी यह संदेह नहीं हुआ कि भारत के इतिहास में वेदांत कभी वेद-द्रोही रहा है अथवा उसमें वेदों का खण्डन किया गया है। उसे इस बात का कभी विश्वास नहीं होता कि एक समय ऐसा भी था, कि उसका अर्थ वर्तमान अर्थ से पूर्णत: भिन्न था जिनके अनुसार वेदांत का अर्थ यह किया जाता था कि इसमें वैदिक विचारों की उपज है और यह ऐसे विचारों का साकार रूप है जो वैदिक साहित्य के अधिमत की परिधि से बाहर है। वास्तव में यही बात थी।
 यह सत्य है कि वेदों और वेदांत के बीच यह विचार भिन्नता 'उपनिषद' शब्द से परिलक्षित नहीं होती थी, जो उस साहित्य की व्यापक पहचान है जो वेदांत दर्शन ने प्रचलित किया और जिसकी व्युत्पति के विषय में बहुत मतभेद हैं।
यह सत्य है कि वेदों और वेदांत के बीच यह विचार भिन्नता 'उपनिषद' शब्द से परिलक्षित नहीं होती थी, जो उस साहित्य की व्यापक पहचान है जो वेदांत दर्शन ने प्रचलित किया और जिसकी व्युत्पति के विषय में बहुत मतभेद हैं।
अधिकांश यूरोपीय विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि उपनिषद् की व्युत्पति "षद्' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, बैठना। इसके पश्चात् "नि" का अर्थ है 'नीचे' और “उप” का अर्थ है, पास, जिसके कारण इसका सम्पूर्ण अर्थ निकलता है, किसी एक व्यक्ति के पास सामूहिक रूप में जाकर बैठना । जैसा कि प्रोफेसर मैक्समूलर ने कहा है, इस व्युत्पति के संबंध में दो आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि इसका आशय उपनिषद सहित इसके अन्य भागों से है और इसकी कभी व्याख्या नहीं की गई कि उसका अर्थ इतना सीमित क्यों निकाला गया ? दूसरी बात है कि उपनिषद् का भाव समागम से मेल नहीं खाता। जब भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके अर्थ हैं- सिद्धांत, गुह्य सिद्धांत अथवा इसका सरलार्थ है, दार्शनिक पुस्तक का शीर्षक, जिसमें गुह्य सिद्धांत निहित हों। मैक्सूमलर के अनुसार तीसरी व्याख्या है, जैसा शंकर ने तैत्तिरीय उपनिषद 2-9 में कहा है कि उपनिषद् में परम आनन्द समाहित है। इस संबंध में मैक्समूलर कहते हैं:
" आरण्यकों में ऐसी व्युत्पत्तियां भरी पड़ी हैं जिनमें वास्तविक अर्थ बताने के स्थान पर शब्द - जाल अधिक है। फिर भी उनसे अर्थ निकालने में सहायता मिलती है।"
मूल अंग्रेजी में 'वेदांत की पहेली' शीर्षक से 21 पृष्ठों की टकित प्रति प्राप्त हुई थी। यह अध्याय पूर्ण लगता है और लेखक द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है। संपादक
बहरहाल, प्रोफेसर मैक्समूलर उपनिषद शब्द का मूल "षद" धातु मानते हैं जिसका अर्थ है विनाश अर्थात् ऐसा ज्ञान जो अज्ञान का विनाश करता है, मोक्ष मार्ग में ब्रह्मलीन होने के लिए संसार का कारण बताता है। प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं कि भारतीय विद्वानों में उपनिषद के इस अर्थ पर सहमति है ।
यदि यह स्वीकर कर लिया जाए कि उपनिषद का वास्तविक अर्थ यही है तो इस सिद्धांत के पक्ष में एक साक्ष्य होगा कि भारतीय इतहास में एक समय था जब वेदांत को विचारों की ऐसी धारा समझा जाता था जिसका वेदों के साथ टकराव हो । परंतु यह बात इस पर निर्भर नहीं है कि इस सिद्धांत के समर्थन के लिए निरुक्ति की सहायता ली जाए। कुछ बेहतर प्रमाण और भी हैं। पहली बात तो यह है कि ‘वेदांत' शब्द का प्रयोग "वेदों के अंतिम ग्रंथ" के रूप में नहीं लिया गया जैसा कि वे हैं। मैक्समूलर¹ का मत है:
“वेदांत एक तकनीकी शब्द है और मूल रूप से इसका अर्थ वेदों का अंतिम अंश नहीं है। और न ही वैदिक साहित्य का अध्याय है, अर्थात् वेदों का अंतिम भाग । तैत्तिरीय आरण्यक (सम्पादक राजेन्द्र मित्र, पृष्ठ 820) जैसे ग्रंथों में कुछ ऐसे अंश हैं। जिनसे भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को भ्रांति हुई है कि वेदांत का सरल-सीधा अर्थ है वेदों का उपसंहार। “यो वेदादू स्वरः प्रकटो वेदांते का प्रतिष्ठितः', ओ३म से वेद का आरम्भ होता है और उसी से वेद का समापन होता है। यहां वेदांत का जो सीधा अर्थ है, वेदादू के विपरीत है, जैसा क इसका अनुवाद किया गया है। उनका अनुवाद वेदांत अथवा उपनिषद असम्भव है। वेदांत दर्शन के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक (पृष्ठ 817) में दिग्दर्शित हुआ है। नारायणी उपनिषद के एक मंत्र में, जिसकी आवृति मुण्डकोपनिषद् 3.2.6 में तथा अन्यत्र भी हुई है " वेदांतविज्ञान सुनिश्चितताः " जो विद्वान वेदांत मर्मज्ञ हैं, उनके अनुसार वह वेदों का उपसंहार नहीं" और श्वेताश्वतर उप 6.22 'वेदांत प्रमाण गुहय्म' नहीं है। भाष्यकार के मत में यह वेद का उपसंहार नहीं जो कालांतर में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है अर्थात् ' क्षुरीकोपनिषद 10 (बिबलि इंड पृ. 210) पुंडारिकेति वेदांतेषु निगाद्यते, वेदांत में छांदोग्य तथा अन्य उपनिषदों को पुण्डरीक कहा गया है। जैसा कि भाष्यकार ने कहा है, परन्तु प्रत्येक वेद का अंतिम ग्रंथ नहीं।
1. दी उपनिषदाज, (एस. बी. ई.) खंड 1 भूमिका ।
इस संबंध में गौतम धर्म सूत्र में स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। अध्याय 19 के 12वें मंत्र में शुद्धीकरण पर गौतम का कथन¹ है:
शुद्धीकरण (पाठ है) उपनिषद्, वेदांत, संहिता सभी वेदों के पाठ हैं आदि-आदि।
इससे यह स्पष्ट है कि गौतम के समय उपनिषद् और वेद अलग-अलग माने जाते थे और वे वेदों का अंग नहीं माने जाते थे। हरदत्त्स ने अपने भाष्य में कहा है, आरण्यक के वे अंश जो (उपनिषद) नहीं हैं, वेदांत कहलाते हैं, यह निर्विवाद साक्ष्य है कि उपनिषद वैदिक सिद्धांतों से भिन्न थे।
भगवद्गीता में वेद के उल्लेख से भी इस विचार को बल मिलता है। भगवद्गीता में 'वेद' शब्द का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। भट्ट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग इस भाव से किया गया है कि लेखक का आशय उपनिषद नहीं है।
उपनिषदों को वेदों के धार्मिक साहित्य से इस कारण विलग किया गया कि उपनिषदों में वेदों की इस शिक्षा का विरोध किया गया है कि धार्मिक कार्य और बलि ही मोक्ष का एक मात्र साधन हैं। कतिपय उपनिषदों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके उनका वेदों के विरुद्ध होना प्रमाणित किया जा सकेगा। मुण्डकोपनिषद् का कथन है:
"देवों में सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता और विश्व परिपालक ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्मज्ञान दिया। (2) अथर्वन ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान अंगिरा मुनि को प्रदान किया। इसके पश्चात्, अंगिरा ने भारद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाह को यह ज्ञान दिया। उसने अपने उत्तराधकारी आंगिरस को यह परम्परा सौंपी, (3) शौनक विधिपूर्वक आंगिरस की शरण में आए और उनसे पूछा 'हे भद्रेय ऋषि वह क्या है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है' (4) आंगिरस ने उत्तर दिया', 'दो विद्याएं प्रसिद्ध हैं। एक परा और दूसरी अपरा' (5) इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसी में स्वरांकन शास्त्रीय व्याकरण भाष्य, पिंगल, गणित और ज्योतिष आते हैं। श्रेष्ठ विज्ञान वह है जो अविनाशी इन्द्रियगोचर होता है। "
1. सैक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट, खंड 2, पृ. 275

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -



