 फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
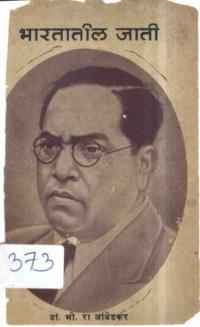
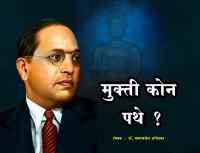
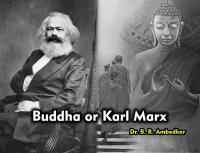
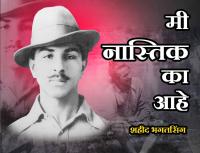
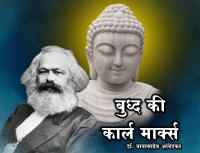
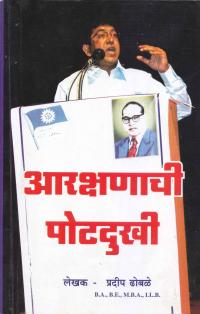

Top News

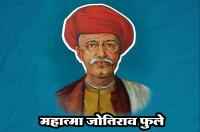


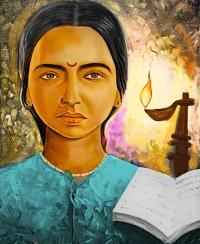

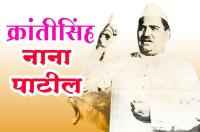
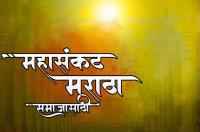
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,विभाग ३ - अहिंसा - भगवान बुद्ध और उनका धम्म (भाग ७१) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर
विभाग ३ - अहिंसा
१. अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार
१. अहिंसा अथवा जीव-हिंसा न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है ।
२. इसका करूणा तथा मैत्री से अत्यन्त निकट का संबन्ध है ।

३. तो भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भवगान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी वा निरपेक्ष थी ? क्या यह एक शील मात्र अथवा एक नियम ?
४. जो लोग भगवान् बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है । उनका कहना है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिये भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिये सद्गुण का ।
५. इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है । यह 'अहिंसा' का प्रश्न सर्वाधिक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न हैं ।
६. बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार व्यवहार किया है ?
७. यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका विचार करना ही होगा ।
८. सिंहल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विराद्ध लड़ने के लिये कहा ।
९. दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिये कहा ।
१०. बर्मा के लोग अण्डा खा लेते हैं मछली नहीं ।
११. अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती हैं।
१२. कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि वे पांच शीलो में से ( जीव - हिंसा से विरत रहने के प्रथम शील को छोड़कर) शेष चार शीलों को ही स्वीकार करेंगे ।
१३. अहिंसा के सिद्धान्त को लेकर ऐसी स्थिति है ।
२. 'अहिंसा' का अर्थ
१. अहिंसा का क्या मतलब है?
२. भगवान् बुद्ध ने कहीं भी 'अहिंसा' की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत की कम अवसरों पर निश्चि शब्दावलि में इस विषय की चर्चा की है ।
३. इसलिये यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्षी से ही भगवान् बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाय ।
४. पहली परिस्थितिजन्य साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान् बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी । ५. यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से सम्बन्धित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है । ६. भगवान् बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था कि भिक्षा में दिये जाने पर भी भिक्षु माँसाहार ग्रहण न करें ।
७. इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह याज्ञों में (ही) पशुहिंसा के विरोधी थे । यह उन्होंने स्वयं कहा है ।
८. ‘अहिंसा परमो धर्मं' यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धान्त है । यह एक जैन सिद्धान्त है । यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं ।
९. एक और साक्षी है जो परिस्थितिजन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से "अहिंसा" की परिभाषा ही है । उन्होनें कहा है -- “सबसे मैत्री करो, ताकि तुम्हे किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पडे" यह अहिंसा के सिद्धान्त के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है ।
१०. इससे ऐसा लगता है कि "अहिंसा' का बौद्ध सिद्धान्त यह नहीं कहता कि 'मारो नहीं' बल्कि यह कहता है कि 'सभी प्राणियों से मैत्री रखो ।”
११. उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि 'अहिंसा' से भगवान् बुद्ध का क्या अभिप्राय था?
१२. यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध 'जीव-हत्या करने की चेतना' और 'जीव-हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे ।
१३. जहा 'जीव-हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया ।
१४. उन्होंने वैसी जीव-हत्या को मना किया जहाँ केवल "जीव हत्या की चेतना " है ।
१५. इस तरह समझ लेने पर "अहिंसा" के बौद्ध सिद्धान्त में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है।
१६. यह एक सोलह आने पक्का, स्थिर नैतिक सिद्धान्त है, जिसका हर किसीको आदर करना चाहिये ।
१७. इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि 'जीव हत्या की आवश्यकता है वा नहीं? व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था? आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिये ।
१८. एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा ।
१९. ब्राह्मणी-धर्म में 'जीव' 'हिंसा करने की चेतना', है ।
२०. जैन धर्म में जीव - हिंसा न करने की चेतना' है ।
२१. भगवान् बुद्ध का सिद्धान्त उनके मध्यम मार्ग के अनुरुप है ।
२२. इसी बात को दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो भगवान् बुद्ध ने शील (Principle) और विनय = नियम (rule) में भेद किया है । उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया। उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है ।
२३. इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करके भगवान् बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात की है ।
२४. एक शील (Principle) तुम्हें कार्य करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ता है। एक नियम (rule) स्वतन्त्र नहीं छोड़ता । या तो तुम नियम को तोड़ते हो, या नियम तुम्हें तोड़ डालता है।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -



