 फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
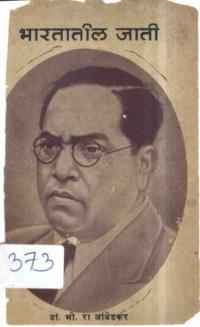
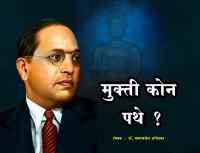
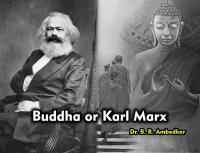
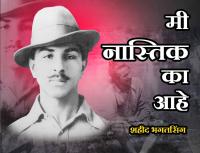
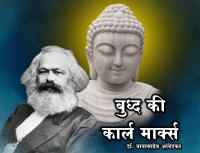
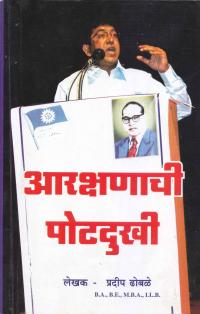

Top News

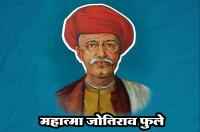


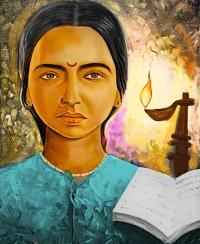

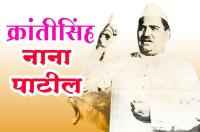
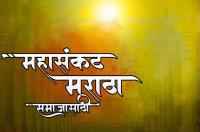
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,भिक्षु तथा ब्राह्मण (भाग ९३) - भगवान बुद्ध और उनका धम्म - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर
३. भिक्षु तथा ब्राह्मण
१. क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अन्तर नहीं ? क्या दोनो एक ही है? - प्रश्न का भी उत्तर नकारात्मक ही है ।
२. इस विषय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी । बुद्ध वचनों में यह जगह जगह बिखरी पडी है । लेकिन उन दोनो में जो अन्तर है, उसे आसानी से एक जगह एकत्र किया जा सकता है ।
३. एक ब्राह्मण,पुरोहित' होता है । उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह मरणादि के अवसर पर, संस्कार, कराना है ।
४. यह, संस्कार, आवश्यक हो जाते है क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलत: पाप में लिप्त है और उसे निर्मल कर निष्याप बनाना है, और क्योंकि, आत्मा, तथा, परमात्मा' का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है ।

५. . इन सब,संस्कारों, के करने-कराने के लिये, पुराहित, होना ही चाहिये । एक भिक्षु न तो किसी, मूल पाप' में विश्वास करता है और न,आत्मा' या,परमात्मा' में । इसलिये उसे कोई संस्कार करने कराने नहीं है । इसलिये एक भिक्षु, पुरोहित' नहीं होता । ६. ब्राह्मण पैदा होता है । भिक्षु बनता है ।
७. ब्राह्मण की जाति होती है । भिक्षु की कोई जाति नहीं होती ।
८. एक बार,ब्राह्मण' के घर पैदा हो गया, जन्म भर के लिये, ब्राह्मण' । कोई, पाप” कोई, जुर्म ऐसा नहीं जो एक, ब्राह्मण' को, अब्राह्मण बना सके ।
९. लेकिन एक बार, भिक्षु, बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि एक भिक्षु जन्म भर के लिये, भिक्षु, ही बना रहे । एक, भिक्षु “भिक्षु बनता है किन्तु यदि वह कभी कोई ऐसी बात कर बैठे कि जो उसे, भिक्षु बने रहने देने के अयोग्य बना दे, तो वह, भिक्षु, नहीं ही रह सकता ।
१०. ब्राह्मण' बनने के लिये किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं । ब्राह्मण से जिस बात की आशा (केवल आशा) की जाती है वह है उसके अपने धार्मिक शास्त्र - ज्ञान की ।
११. भिक्षु की बात इसके सर्वथा प्रतिकूल है । मानसिक तथा नैतिक शिक्षण उसका जीवन--प्राण है।
१२. एक ब्राह्मण जितनी चाहे उतनी सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है । एक भिक्षु नहीं कर सकता ।
१३. यह कोई छोटा फर्क नहीं है । आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतन्त्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी-- सम्पत्ति कडे से कडे प्रतिबन्ध का काम करती है । इससे दो प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है । इसीलिये ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिये परिवर्तन का मतलब है शक्ति की हानि, धन की हानि ।
१४. सम्पत्ति-विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतन्त्र होता है । कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके ।
१५. ब्राह्मण होते हैं ।लेकिन हर ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता है । कोई ऐसा धार्मिक संघठन नहीं, जिसके वह अधीन हो ।हर ब्राह्मण अपना कानून आप है । हाँ ब्राह्मण आपस में भौतिक स्वार्थो से अवश्य बन्धे हुए है ।
१६. दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है । यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य न हो । भिक्षु आप अपना कानून नहीं होता । वह, संघ' के अधीन होता है।, संघ' एक आध्यात्मिक संगठन है ।
४. भिक्षु और उपासक
१. सद्धम्म ने भिक्षु के, धम्म' और उपासक के, धम्म' में स्पष्ट रुप से विभाजक रेखा खींची है ।
२. भिक्षु को पत्नि-विहीन रहना ही होगा । उपासक को नहीं । वह शादी कर सकता है ।
३. भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता । भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता । उपासक के लिये यह आवश्यक नहीं है । उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है।
४. भिक्षु की कोई सम्पत्ति नहीं हो सकती । लेकिन गृहस्थ की सम्पत्ति हो सकती है - वह सम्पत्ति रख सकता है।
५. भिक्षु के लिये प्राणि-हत्या अनिवार्य तौर पर वर्जित है । गृहस्थ के लिये नहीं । वह (अवस्था - विशेष में) जीव-हत्या कर भी सकता है।
६. यूं पंचशील के नियम दोनों के लिये समान है । लेकिन भिक्षु के लिये वे व्रत रुप है । वह उन्हें तोडेगा तो दण्ड का भागी होगा ही । उपासक (गृहस्थ) के लिये वे अनुकरणीय शील- मात्र है।
७. भिक्षु के लिये पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है । गृहस्थ के लिये उसके अपने विवेक पर निर करता है ।
८. तथागत ने दोनों के, धम्म' में ऐसा भेद क्यों रखा? इस के पीछे कोई न कोई खास कारण होना चाहिए क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे ।
९. कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रुप से नहीं कहा है । यह हमारे अनुमान का विषय है । तो भी यह आवश्यक है कि इस विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट समझ में आ जाय ।
१०. इस में कोई सन्देह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म- राज्य स्थापित करना चाहते थे । इसलिये उन्होंने सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया - भिक्षुओ को भी, गृहस्थों को भी ।
११. लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्व सामान्य आदमियों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे उस आदर्श समाज की स्थापना न कर सकेंगें जिसका आधार एकमात्र, धम्म' होगा ।
१२. आदर्श के लिये, व्यवहारिक' होना आवश्यक है । इतना ही नहीं लोगों को वह व्यवहारिक, लगाना भी चाहिये । तभी लोग उस तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं।
१३. इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरम्भ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने उस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ स्वरुप हो, जिस से सर्व - सामान्य जनता भी यही समझा सते कि, आदर्श, कोई, अव्यावहारिक' नही था, बल्कि ऐसा था कि जो साकार हो सके ।
१४. तथागत ने जिस, धम्म' का उपदेश दिया, संघ उसी का एक साकार सामाजिक नमूना है ।
१५. यही कारण है कि भगवन बुद्ध ने एक भिक्षु के, धम्म, और एक उपासक (गहस्थ) के धम्म में यह विभाजक रेखा खींची । भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल भी था और उपासक को यथा सामर्थ्य उसका अनुकरण करना था ।
१६. एक प्रश्न और भी है और वह यह कि भिक्षु का जीवन-कार्य क्या है ?
१७. क्या भिक्षु-जीवन व्यक्तिगत साधना के लिये ही है अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्ग-दर्शन भी करना ही है? १८. ये दोनों ही उसके जीवन-कार्य है ।
१९. बिना व्यक्तिगत-साधना के वह नेतृत्व कर नहीं सकता । इसलिये उसे अपने में एक सम्पूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, धाम्मिक और ज्ञान- सम्पज्ञ व्यक्ति बनना ही होगा । इसके लिये उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी ।
२०. एक भिक्षु गृह त्याग करता है । वह संसार त्याग नहीं करता । वह अपने घर को इसलिये छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त है, और जो दुःख में पडे हैं, जो चिन्ता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है ।
२१. करुणा--जो कि धम्म का सार है--का तकाजा है कि हर आदमी दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे । भिक्षु भी इस का अपवाद नहीं ।
२२. व्यक्तिगत-साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो यदि कोई भिक्षु, पीडित मानवता की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है ।वह दुसरा और कुछ भी हो सकता है; किन्तु वह भिक्षु नहीं ही है ।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -



