 फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
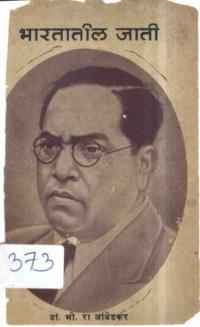
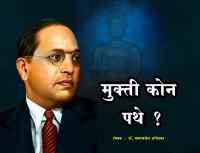
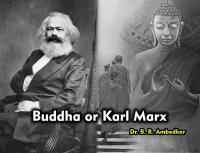
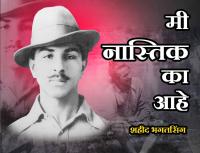
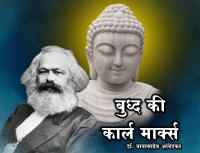
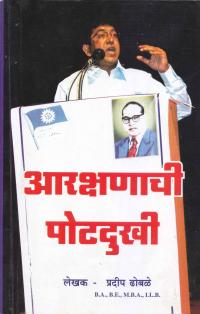

Top News

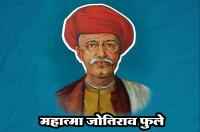


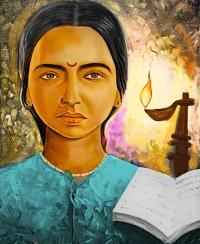

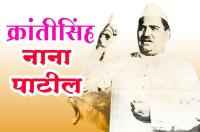
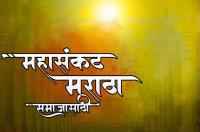
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,पाचवा भाग : बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती - भगवान बुद्ध और उनका धम्म (भाग १८) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर
पाचवा भाग : बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती
१. बुद्ध और वैदिक ऋषि
१. वेद, मंत्रों अर्थात् ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है । इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को 'ऋषि' कहते हैं ।
२. मन्त्र देवताओं को सम्बोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है जैसे, इन्द्र, वरूण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म महद्धि, यम तथा अन्य ।

३. प्रार्थनयें प्रायः शत्रुओं से रक्षा वा शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिये हैं, धन प्राप्ति के लिये हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेट स्वीकार करने के लिये हैं ।
४. वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है । लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है ।
५. इन वैदिक ऋषियों के नाम है: (१) अधमर्षण, (२) प्रजापति परमेष्ठी, (३) ब्रह्मणस्पति वा बृहस्पति, (४) अनिल, (५) दीर्घतमा, (६) नारायण, (७) हिरण्यगर्भ तथा (८) विश्वकर्मा ।
६. इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्यायें थीं: यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ? अलग-अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गई ? उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है ? किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की ? यह संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जायेगा ?
७. अधमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस (ताप) से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व हैं जिससे नित्य धर्म और ऋत (सत्य) की उत्पत्ति हुई है । इन्हीं से तम ( अंधकार, रात्रि) की उत्पत्ति है । तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की । काल से ही सूर्य तथा चन्द्रमा पैदा हुए तथा द्यौ और पृथ्वी ने जन्म धारण किया । काल ने ही अन्तरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की ।
८. ब्रह्मणस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत के सत रूप में आई । असत् से कदाचित उसका आशय अनंत से था । सत् मूल रूप से असत् से ही उत्पन्न हुआ । समस्त सत् का मूलाधार असत् ही था और समस्त भावी सत् का तो इस समय असत् है ।
९. प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत् की उत्पत्ति असत् से हुई ? उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं । उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है । उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार --जल है वह न सत् के अन्तर्गत आता है और न असत् के
१०. परमेष्ठी ने जडतत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची । उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न-भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है । उसने इस निहित- -तत्व को 'काम' कहा है -- विश्व व्यापी इच्छा- शक्ति ।
११. एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल । उसके लिये वायु ही मुख्य तत्व था । इसमें चलन अन्तर्निहित था । उसीमें उत्पन्न करने की शक्ति है।
१२. दीर्घतमा का मत था कि अन्त में सभी चिजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अन्तर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है ।
१३. सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि ।
१४. सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजाकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घतमा का मत था ।
१५. नारायण के मत के अनुसार पुरूष ही जगत का आदि कारण है । पुरुष से ही सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, , वायु, अन्तरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं ।
१६. हिरण्य-गर्भ सिद्धान्त की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्ठी और नारायण के बीच में था । हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्ण- गर्भ । यही विश्व की वह महान् शक्ति थी, जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था ।
१७. हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है । यह अग्नि ही है जो सौर - र मण्डल का उपादान कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति ।
१८. विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना की जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उसका स्वभाव- धर्म ही है, योग्य नहीं था । यदि हम जल को ही मूल अपादान मानें तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज, आदि की यह शक्तियाँ, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आये ?
१९. विश्वकर्मा का कहना था कि 'पुरुष' ही है जो सब किसी का मूलाधार है । 'पुरुष' आदि में हैं, 'पुरुष' अन्त में है । वह इस दृश्य संसार के पहले से है, इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है । अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है । पुरुष एक और केवल एक है। वह अज है और उसीमें सभी उत्पन्न चीजों का निवास है । वही है जिसका चेतस भी महान् है और सामर्थ्य भी महान है । वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब के अन्त से परिचित हैं ।
२०. बुद्ध सभी वैदक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे । वह उनमें से कोई दस ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मन्त्र रचयिता मानते थे ।
२१. लेकिन उन मन्त्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके ।
२२. बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कान्तार के समान निष्प्रयोजन थे ।
२३. इसलिये 'बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनमें कुछ सीखा जा सके वा ग्रहण भी किया जा सके ।
२४. इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था । निस्संदेह उन्हें (ऋषियो को ) सत्य की खोज थी । वे उसे अन्धेरे में टटोल रहे थे। किन्तु उन्हें सत्य मिला न था ।
२५. उनके सिद्धान्त केवल मानसिक उड़ाने थी, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई सम्बन्ध न था । दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नये सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी ।
२६. इसलिये उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी सम्पूर्ण रूप से अवहेलना की ।
२. कपिल दार्शनिक
१. प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है ।
२. उसका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था । वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था ।
३. उसका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था ।
४. सत्य के लिये प्रमाण आवश्यक है । सांख्य का यह प्रथम सिद्धान्त है । बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं ।
५. सत्य को सिद्ध करने के लिये कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किये -- (१) प्रत्यक्ष और अनुमान ।
६. प्रत्यक्ष से मतलब है (इन्द्रियों के माध्यम से) विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी ।
७. अनुमान तीन प्रकार का है -- १) कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है; (२) कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं; ३) सामान्यतोदृष्ट अनुमान, जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान- परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न-भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं ।
८. उसका अगला सिद्धान्त सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में था । सृष्टि की उत्पति और उसका कारण ।
९. कपिल को किसी सृष्टि-कर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था । उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है जैसे मिट्टी से बरतन बनता है अथवा धागों से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है ।
१०. यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान्य न था ।
११. उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिये हैं ।
१२. असत् कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता । वास्तव में नई उत्पत्ती कुछ होती ही नहीं । वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है, वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है । किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है । और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है ।
१३. तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है?
१४. कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप है -- १) व्यक्त (विकसित) तथा अव्यक्त (- अविकसित )
१५. व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती ।
१६. व्यक्त वस्तुएँ ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्त्रोत बमेल हैं ।
१७. तमाम व्यक्त वस्तुएँ परस्पर समान होतीं हैं । इसलिये कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती । और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिये वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकतीं ।
१८. कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिज्ञ होना ही चाहिये । यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ह है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अन्तिम कारण नहीं हो सकता । इसे किसी अन्तिम कारण का परिणाम होना चाहिये । १९. जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी किया इन्द्रिय-गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था-
२०. यह अनेक कारणों से हो सकता है । हो सकता है अनेक दूसरी अतिसूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्याधिक दूरी के कारण अनुभुति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तिसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो; अथवा किसी तीव्रतर वेदना (अनुभूति) के कारण अनुभुति न होती हो, अथवा अन्धेपन वा किसी अन्य इन्द्रिय-दोष के कारण अनुभूति न होती हो अथवा द्रष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति होती हो ।
२१. जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है? विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त-रूप में क्या अन्तर है?
२२. कपिल का उत्तर था -- “ व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है। लेकिन दोनों के मूल स्त्रोत स्वतन्त्र हैं और उनका कोई कारण नहीं ।"
२३. व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है । वे देश काल से सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्व व्यापक है । व्यक्त वस्तुएँ क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं ।
२४. कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है । वे तीन गुण हैं, सत्व, रज, तम ।
२५. इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात् सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है; दूसरा गुण रज है जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है; तीसरा गुण तम है जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो अपेक्षा वा निष्क्रियता को उत्पन्न करता है ।
२६. तीनों गुण परस्पर सम्बद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। वे एक दूसरे के सहायक होते है । वे एक दूसरे से मिले रहते हैं । जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते है ।
२७. जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते है, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता ।
२८. जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरम्भ हो जाता है।
२९. यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी - बेशी क्यों हो जाती है, कपिल का उत्तर था कि उसका कारण दुःख है । ३०. कपिल के दर्शन सिद्धान्त कुछ-कुछ ऐसे ही थे ।
३१. अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धान्तो से ही विशेष रूप से प्रभावित थे ।
३२. कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षायें बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ-कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ी ।
३३. लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया । कपिल की उन्हें केवल तीन ही बातें: ग्राह्य थी I
३४. उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिये । यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिये ।
३५. उन्हे यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल वा यथार्थताश्रित कारण विद्यमान नहीं है ।
३६. उन्हें यह बात मान्य थी कि संसार में दुःख है ।
३७. कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की क्योंकि उनका उनके लिये कोई उपयोग न था ।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -



