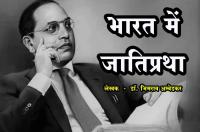फुले - शाहू - आंबेडकर
फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar
Top Books
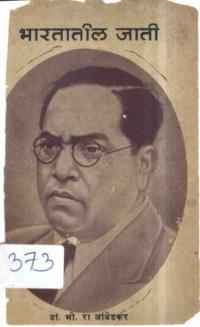
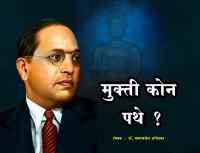
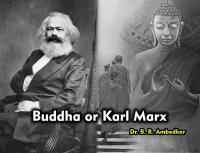
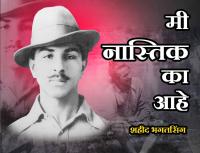
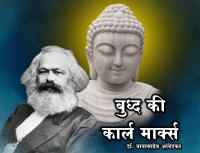
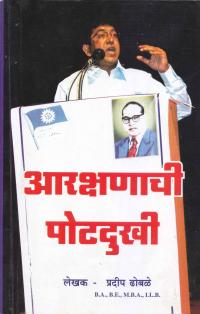

Top News

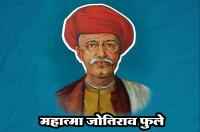


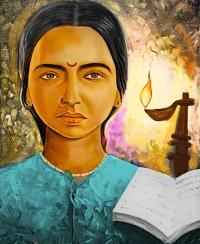

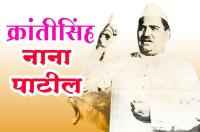
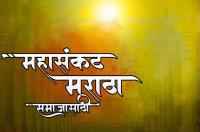
Labels
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,लाहौर जातपांत तोड़क मंडल १९३६ के वार्षिक सम्मेलन के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया भाषण
4
खेद है कि आज भी जातिप्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक हैं। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जातिप्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जातिप्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के विरुद्ध पहली बात यह है कि जातिप्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है यह श्रमिकों का विभाजन भी है। इसमें संदेह नहीं है कि सभ्य समाज को श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है। किन्तु किसी भी सभ्य समाज में श्रम के विभाजन के साथ इस प्रकार के पूर्णतः अलग वर्गों में श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन नहीं होता । जातिप्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन के साथ श्रमिकों को इस प्रकार का क्रम नहीं होता। जातिप्रथा के इस विचार के विरुद्ध एक तीसरा तथ्य भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं होता। यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित नहीं है। सामाजिक और वैयक्तिक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिन्दु तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। जातिप्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि माता-पिता के सामाजिक स्तर पर होता है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसायों का यह स्तरण जो जातिप्रथा का परिणाम है, निश्चय ही घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होता। इसमें तेजी से और अचानक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तनों से व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपने आपको ढालने की ऐसी स्वतंत्रता के बिना, उसके लिए अपनी आजीविका कमाना असंभव हो जाएगा। जातिप्रथा हिन्दुओं को ऐसे व्यवसाय अपनाने की अनुमति नहीं देगी, जहां उनकी जरूरत है, यदि वे आनुवंशिक रूप से उनसे संबंधित नहीं हैं। यदि कोई हिन्दु अपनी जाति के लिए निर्धारित पेशे के अलावा नए पेशे को अपनाने की बजाय भूखा मरता दिखाई देता है, तो उसका कारण जातिप्रथा की कठोरता ही है। पेशों के पुनर्समायोजन की छूट न देकर अधिकतर बेरोजगारी फैलती है, जिसका सीधी कारण जातिप्रथा है, जो हमारे देश में मौजूद है। श्रम के विभाजन के रूप में जातिप्रथा में एक और गंभीर दोष है । जातिप्रथा द्वारा उत्पन्न श्रम का विभाजन छांट पर आधारित विभाजन नहीं है। इसमें वैयक्तिक भावना और वैयक्तिक वरीयता का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार पूर्व-नियति का सिद्धांत है। सामाजिक कार्यकुशलता का विचार हमें इस बात को स्वीकार करने पर विवश करता है कि औद्योगिक प्रणाली में सबसे बड़ा दोष केवल निर्धनता नहीं है। इस प्रणाली में जो बड़ा कष्ट है, वह यह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं, जिनके प्रति उनकी प्रवृत्ति नहीं है। यदि किसी ऐसे को व्यवसाय से निरंतर लगा रहना पड़े तो उस व्यक्ति को उससे पीछा छुड़ाने, उसके प्रति सद्भावना न होने और उससे बचने की इच्छा होती है। भारत में अनेक ऐसे व्यवसाय हैं, जिन्हें हिन्दू निकृष्ट मानते हैं, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं, वे उनसे पीछा छुड़ाने को आतुर रहते हैं। ऐसे व्यवसायों से बचने और उन्हें त्यागने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसका एकमात्र कारण वह निराशाजनक प्रभाव है, जो उन पर हिन्दू धर्म द्वारा उनके ऊपर आरोपित कलंक के कारण पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में क्या कार्यकुशलता हो सकती है, जिसमें न तो लोगों के दिल और न दिमाग अपने काम में होते हैं? इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जातिप्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक शक्तियों का दमन रहता है और सामाजिक नियमों की तत्कालीन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति होती है।

5
कुछ लोगों ने जातिप्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित रखना है। अब नृजाति वैज्ञानिकों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है, विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो यह स्थिति आवश्यक है। श्री डी. आर. भंडारकर ने "हिन्दू जनसंख्या में विदेशी तत्व" (फोरन एलीमेंट्स इन द हिन्दू पॉपूलेशन) विषय पर अपने प्रलेख में कहा है कि "भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी, जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में हैं कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं।" जातिप्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। वास्तव में, जातिप्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। यह मानना कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजाति की वास्तविक विभिन्नताएं और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थीं, तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना है।
पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जातीय संबंध है? बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जातीय संबंध है? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या जातीय अंतर है? मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पेरिया में क्या जातीय अंतर है? जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है, जिसका पंजाब का चमार है, और मद्रास के ब्राह्मण की वही जाति है जो मद्रास के पेरिया की । जातिप्रथा मानव- वंश या प्रजाति के विभाजन के निर्धारण नहीं करती। जातिप्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि यह मान लिया जाए कि जातिप्रथा मानव प्रजाति को विभाजित कर देती है तो यह भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग-अलग जाति और रक्त के समुदायों को अंतर्विवाह करने की अनुमति दी तो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों को एक-दूसरे में समागम से क्या हानि होगी? इसमें संदेह नहीं कि जहां तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, उनमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान इन्हें दो अलग-अलग जीव-रूपों की मान्यता देता है, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता (मिश्रण - हीनता) में विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ यह नहीं कहते हैं कि अलग-अलग प्रजाति के लोग अलग-अलग किस्म के होते हैं। वे सभी एक ही नस्ल की अलग-अलग किस्मों के होते हैं। वे एक-दूसरे की उप-जातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं ऐसी संतानें, जो स्वयं भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी, और जो बंध्या न होंगी। जातिप्रथा के पक्ष में आनुवंशिकता और सुजननिकी की तर्कहीन बातें बताई जाती हैं। अगर जातिप्रथा सुजननिकी (यूनिक्स) के मूलभूत सिद्धांत के अनुकूल होती तो इसमें किसी को आपत्ति न होती, क्योंकि किसी को भी उत्तम व्यक्तियों द्वारा समागम से जाति की किस्म में सुधार लाने में आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जातिप्रथा के कारण उत्तम स्त्रियों और पुरुषों में सही समागम किस प्रकार सुनिश्चित होता है। जातिप्रथा नकारात्मक तथ्य है। यह केवल अलग-अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर्विवाह का निषेध करती है। यह ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है, जिससे एक ही जाति के दो उत्तम नर-नारी आपस में विवाह कर सकें। यदि जाति का उद्गम सुजननिकी के सिद्धांत पर आधारित है, तो उप-जातियों का प्रादुर्भाव भी सुजननिकी के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरतापूर्वक यह कह सकता है कि उप-जातियों का उद्गम सुजननिकी के कारण हुआ है? मैं समझता हूं कि स्पष्ट कारणों से ऐसा मानना बहुत ही असंगत है। अगर जाति का आशय प्रजाति या नस्ल से है, तो उप-जातियों में पाए जाने वाले अंतर को प्रजातीय अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब उप-जातियां भी उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नस्ल की उप खंड होंगी। इससे स्पष्ट है कि उप जातियों में आपस में रोटी-बेटी के व्यवहार पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रजाति या रक्त की शुद्धता बनाए रखना नहीं हो सकता। फिर यदि उप-जातियों का उद्गम सुजननिकी ही हो सकता, तो इस कथन में कोई दम नहीं है कि प्रजाति का उद्गम सुजननिकी है। फिर अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति का उद्गम सुजननिकी के प्रयोजन से है, तो अंतर्विवाह संबंधी निषेध समझ में आ जाता है। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उप जातियों के बीच खान-पान पर भी निषेधाज्ञा लगाने का क्या प्रयोजन है? आपस में खान-पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी। इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है। और जो इसे सुजननिकी के आधार पर सही बताना चाहते हैं, वे विज्ञान का नाम लेकर घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सुजननिकी को व्यावहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक हमें आनुवंशिकता के नियमों का पक्का ज्ञान न हो जाए। प्रो. बेटसन अपनी पुस्तक 'मेंडेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हैरिडिटी' में कहते हैं, "यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं, या जो शारीरिक शक्ति उसमें अधिक मात्रा में है, वह अनेक कारणों के होने से घटित है, न केवल एक आनुवंशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण।" यदि यह तर्क दिया जाए कि जातिप्रथा सुजननिकी की परिकल्पना का परिणाम था, तो उसका आशय वह होगा कि आज के हिन्दुओं के पूर्वज आनुवंशिकता के विषय में उस ज्ञान से संपन्न थे, जो आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पेड़ की जांच उसके फलों से की जानी चाहिए। अगर जाति सुजननिकी के आधार पर होती, तो उससे किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे? जहां तक शारीरिक क्षमता का संबंध है, उसमें हिन्दू प्रजाति सबसे घटिया किस्म (सी-3) की है। वह छोटे आकार के बोनों की जाति है, जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और जिनमें 'दम' नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है, जिसकी नब्बे प्रतिशत जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है। कि जातिप्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सुजननिकी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । जातिप्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जो हिन्दू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जातिप्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर-जबरदस्ती के बल पर अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया ।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर
You might like This Books -